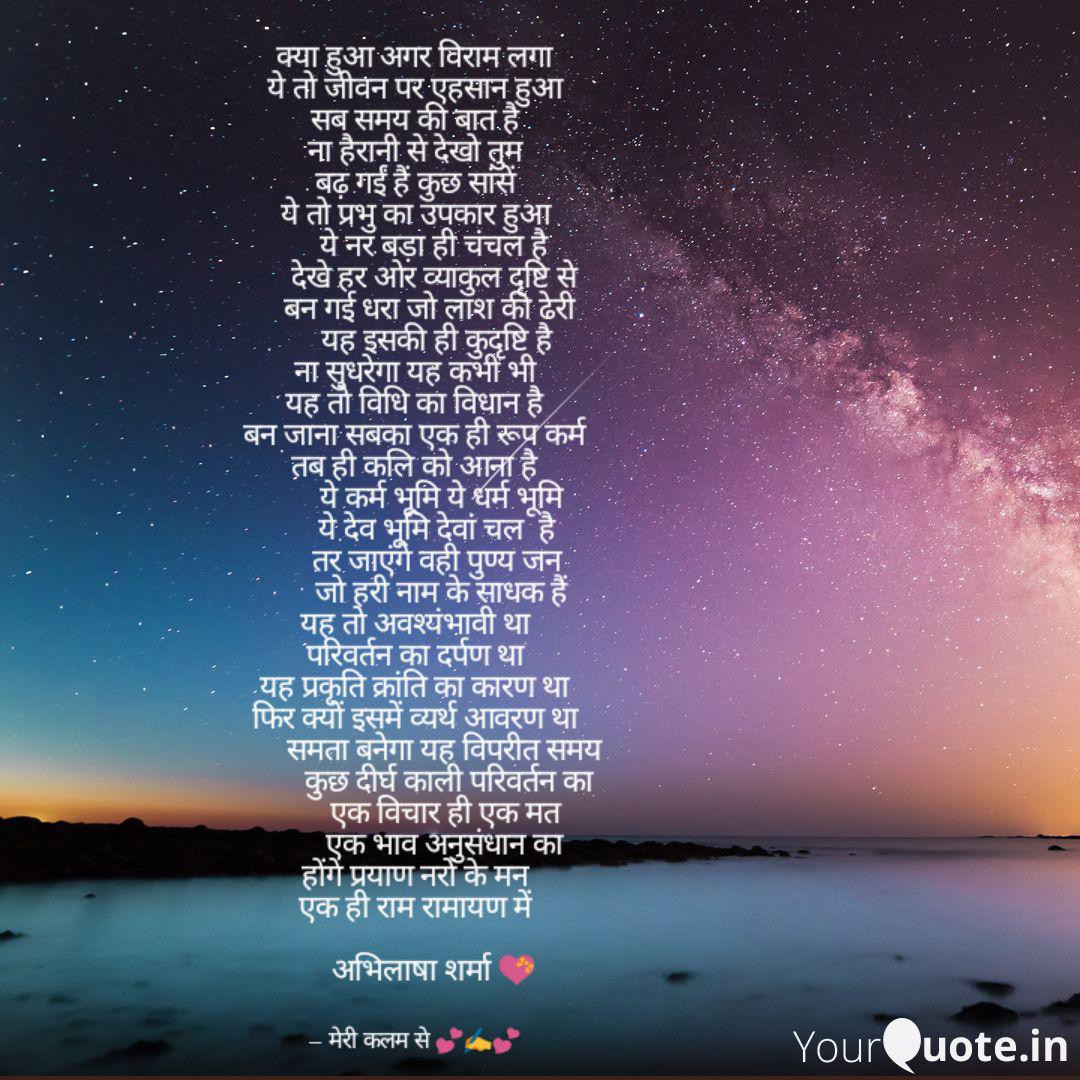जो जैसा सोचता और करता है, वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा, वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे, वैसे कर्म बनेंगे और जैसे कर्म करेंगे, वैसी परिस्थितियां बन जाएँगी। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। वास्तविक शक्ति “साधनों” में नहीं, “विचारों” में सन्निहित है।
कहते हैं मनुष्य के भाग्य का लेखा-जोखा कपाल में लिखा रहता है। कपाल अर्थात् मस्तिष्क । मस्तिष्क अर्थात विचार। अतः मानस शास्त्र के आचार्यों ने यह उचित ही संकेत किया है कि भाग्य का आधार हमारी विचार पद्धति ही हो सकती है। विचारों की प्रेरणा और दिशा अपने अनुरूप कर्म करा लेती है। इसीलिए भी कहते हैं कि “मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ।

विचार आंतरिक बल और पुरुषार्थ है, उसे जिस लक्ष्य पर नियोजित किया जाता है, उसी में तदनुरूप प्रगति होती है और सफलता मिलती है। लोग अस्त-व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझाए रहकर उसे नष्ट भी करते हैं और विकृतियों में उलझकर – अपने लिए संकट भी उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य तक पहुँचने का पुरुषार्थ इंद्रिय शक्ति के माध्यम से ही करना पड़ता है और उसी आधार पर सफलताएँ प्राप्त होती हैं, पर इंद्रिय शक्ति को पकड़कर विशेष दिशा में लगा देने का पुरुषार्थ “विचार बल” द्वारा ही संभव होता है। सही दिशा में इंद्रिय शक्ति न लग पाने से उपलब्धियाँ नहीं मिलतीं। बात यहीं तक सीमित नहीं, विचार बदलते हैं तो इंद्रियाँ भी दिशा बदलती हैं और हजार परेशानियाँ मनुष्य स्वयं पैदा कर लेता है। रावण प्रकांड पंडित, विद्वान, ज्ञानी था, लेकिन उसने सत्पुरुषों जैसा व्यवस्थित चिंतन छोड़ दिया, लोलुपों का अस्त-व्यस्त क्रम अपनाया। इसलिए अपने ज्ञान का ठोस लाभ समाज को न दे सका। आदर्शनिष्ठ चिंतन छोड़कर, संकीर्ण स्वार्थगत चिंतन में, हीन कर्मों में लगा दिया और दुर्गति करा ली। उसकी रुचि के और संसार की आवश्यकता के ढेरों कार्य प्रतीक्षा में ही रखे रह गए।
“विचार” सूक्ष्म स्तर का कर्म है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार – प्रवाह को भी सत्प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार – प्रवाह को भी सुनियोजित कर, लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है ।
जय श्री राधे